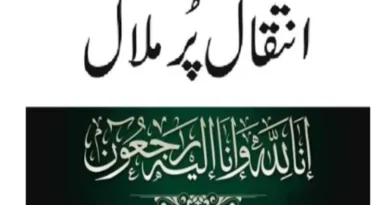भारत ने ताक़त दिखाने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी उजागर हो गई
यूसुफ़ नज़र
10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच एक “पूर्ण और तत्काल” संघर्षविराम की घोषणा की, जिसे उनकी प्रशासन ने मध्यस्थता कर के संभव बनाया। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि जैसे ही खुफिया रिपोर्टों ने हालात के और बिगड़ने के संकेत दिए, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ़ स्टाफ सुसी वाइल्स ने तत्काल कूटनीतिक दख़ल की पहल की। वेंस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संभावित विनाशकारी नतीजों के प्रति चेतावनी दी और भारत-पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत को प्रोत्साहित किया।
इस संघर्षविराम की घोषणा से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। एक परमाणु युद्ध की आशंका—जो एक 2019 के अध्ययन के अनुसार एक हफ्ते में ही 12.5 करोड़ लोगों की जान ले सकता है—ने पूरे क्षेत्र में चिंता पैदा कर दी थी और अमेरिकी कूटनीति को सक्रिय कर दिया।
हालांकि भारत में, ट्रंप की यह घोषणा कुछ हलकों में अलग नज़रिए से देखी गई। भारत के पूर्व सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने एक्स पर लिखा: “संघर्षविराम 10 मई 25: भविष्य में भारत का इतिहास यह पूछेगा कि इसके सशस्त्र और कूटनीतिक प्रयासों से कौन से रणनीतिक लाभ मिले।” सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उसी मंच पर लिखा: “काश संघर्षविराम की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री @narendramodi करते, न कि किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष ने। हमने शिमला (1972) समझौते के बाद से ही तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का विरोध किया है। अब हमने इसे क्यों स्वीकार कर लिया? मुझे उम्मीद है कि कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण नहीं होगा, क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है।”
ओवैसी की टिप्पणी शायद ट्रंप के उस बयान की ओर इशारा करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह “भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर यह देखना चाहते हैं कि क्या हज़ार साल बाद कश्मीर पर कोई समाधान निकल सकता है।”
भारत में कुछ लोग इस संघर्षविराम को मोदी सरकार की अमेरिकी दबाव में हुई वापसी के रूप में देख रहे हैं, जबकि कश्मीर पर मध्यस्थता की अमेरिकी पेशकश को भारत की वर्षों पुरानी “तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप” की अस्वीकृति में एक दरार के तौर पर देखा जा रहा है।
दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में धारणाएं अक्सर वास्तविकताओं से आगे निकल जाती हैं—जब तक कि वास्तविकता खुद न टकरा जाए। भारत ने वर्षों तक अपनी आर्थिक प्रगति और परमाणु शक्ति के बल पर क्षेत्रीय वर्चस्व का दावा किया है। लेकिन 22 अप्रैल को कश्मीर में ‘रेज़िस्टेंस फ्रंट (TRF)’ द्वारा किए गए नरसंहार के बाद उसकी प्रतिक्रिया ने उसकी कमजोरी उजागर कर दी। ताक़त दिखाने की मंशा से शुरू की गई कार्रवाई अंततः पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति को मज़बूत कर गई और मोदी सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर असहज बना दिया।
7 मई को भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य TRF जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को नष्ट करना था। इस ऑपरेशन में फ्रांस निर्मित राफेल विमानों का इस्तेमाल किया गया और इसका मकसद प्रधानमंत्री मोदी की मज़बूत नेता की छवि को और मजबूत करना था। लेकिन इसके परिणाम विवादित रहे। पाकिस्तान ने आम नागरिकों की मौत का दावा किया, जबकि भारत का कहना है कि केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया।
पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई में अपने जेट तैनात किए और दावा किया कि उसने भारत के पांच लड़ाकू विमान, जिनमें तीन राफेल शामिल थे, गिरा दिए। दो अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि एक चीनी J-10 विमान ने कम से कम दो भारतीय विमान गिराए, जिसमें उसे चीनी खुफिया और निगरानी प्रणाली का सहयोग मिला। भारत ने इन नुकसानों को स्वीकार नहीं किया।
शुरुआत में भारतीय मीडिया ने कराची के बंदरगाह समेत पाकिस्तानी शहरों पर भयानक हमलों के दावे किए, लेकिन ये खबरें बाद में गलत और प्रोपेगैंडा साबित हुईं।
9 मई को भारत ने इस्लामाबाद के पास स्थित पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर मिसाइल हमले किए, ऐसा पाकिस्तान का दावा है। जवाब में पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के अड्डों—उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज—पर कम दूरी की मिसाइल और ड्रोन हमले किए। भारतीय वायुसेना की अधिकारी व्योमिका सिंह ने पुष्टि की कि इन हमलों में सैन्य और नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा।
पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान को चीन से सैन्य सहयोग में भारी वृद्धि हुई है। 2020 से अब तक पाकिस्तान की 81% सैन्य आपूर्ति चीन से हो रही है।
कई भारतीय रक्षा विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि चीन के समर्थन वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य तैयारियां पर्याप्त नहीं हैं, खासकर जब अमेरिका और रूस से सीमित समर्थन मिल रहा हो। कुछ विशेषज्ञों ने भारत की विदेश नीति की आलोचना की, जो चीन-पाकिस्तान के बीच बढ़ती निकटता को रोकने में विफल रही। लेकिन नई दिल्ली ने इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया।
बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने भारत की रणनीतिक सीमाएं उजागर कर दीं। अब नई दिल्ली की तत्काल प्रतिक्रिया शायद रक्षा बजट बढ़ाने और कश्मीर में सैन्य उपस्थिति को और मजबूत करने की हो।
लेकिन भारत को यह समझने की ज़रूरत है कि छाया युद्ध और छिपी हुई आक्रामकता के इस सिलसिले से क्षेत्रीय अस्थिरता बनी रहेगी। भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां वर्षों से अपने-अपने एजेंटों और संगठनों के माध्यम से कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक तनाव को हवा देती रही हैं।
आगे का रास्ता इस बात पर निर्भर करता है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद अब कितनी समझदारी से निर्णय लेते हैं। अब ज़रूरत बयानबाज़ी की नहीं, बल्कि संयम की है। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो यह भू-राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक मंदी और लाखों लोगों के लिए संकट ला सकता है। दुनिया की एक चौथाई गरीब आबादी और 35 करोड़ निरक्षर वयस्कों वाले भारत और पाकिस्तान लम्बे संघर्ष का बोझ नहीं उठा सकते। यह तनाव न केवल भारत की आर्थिक वृद्धि को पटरी से उतार सकता है, बल्कि पाकिस्तान की जर्जर अर्थव्यवस्था को भी पूरी तरह बर्बाद कर सकता है।